दो जोली, एक अदालत: पुरानी बनाम नई, और बीच में जनता की आवाज़
Jolly LLB 3 रिव्यू का सबसे बड़ा हुक यही है—दो अलग दुनिया के जोली, एक ही कोर्टरूम में। एक तरफ कानपुर की ठसक, दूसरी ओर मेरठ की ठाठ; टकराव मज़ाक में नहीं, दिमाग और दिल दोनों के इम्तिहान में बदलता है। ये सेट-अप किसी दिखावे जैसा हो सकता था, पर फिल्म इसे अपने सबसे दमदार औज़ार की तरह इस्तेमाल करती है।
निर्देशक सुभाष कपूर फ्रैंचाइज़ के तीसरे भाग में उस चीज़ को वापस लाते हैं जिसकी वजह से यह सीरीज़ खास बनी—व्यंग्य और संवेदना का संतुलन। पंचलाइन सिर्फ हंसाने के लिए नहीं, सवाल उठाने के लिए आती है। कोर्टरूम में हर बहस के पीछे एक सामाजिक संदर्भ बैठा है—इस बार केंद्र में किसानों के अधिकार, जमीन के कब्जे और सिस्टम से जूझती आम-आदमी की लड़ाई है।
अक्षय कुमार और अरशद वारसी के बीच की केमिस्ट्री फिल्म की रफ्तार तय करती है। दोनों की अदाएं, शहरों का टोन और पेश-तरकीबें अलग हैं, लेकिन तकरार कहीं भी कड़वाहट में नहीं बदलती। जोली बनाम जोली का खेल ह्यूमर से लबालब है, पर पंच के नीचे एक चुभता सच लगातार बना रहता है—कानून किताबों में बराबरी का वादा करता है, पर हकीकत में बराबरी तक पहुंचना कईयों के लिए लक्ज़री है।
और हां, सौरभ शुक्ला फिर से कोर्ट के मालिक दिखते हैं। उनका जज किरदार सख्त भी है और शरारती भी, और हर बार जब वे बोलते हैं, दृश्य अपने आप उठ खड़ा होता है। टाइमिंग की सटीकता, आंखों का भाव और एक तटस्थ, मानवीय दृष्टि—ये तीनों मिलकर अदालत को मचाने की जगह समझने का मंच बना देते हैं।
फिल्म का लेखन खास है क्योंकि यह उपदेश नहीं देता। किसान-ज़मीन जैसे संवेदनशील मुद्दे संवादों में घुलाए गए हैं—कभी एक तंज, कभी एक करारा सवाल, और कभी एक छोटी, निजी हार-जीत की कहानी। दर्शक हंसता भी है, ताली भी बजाता है, और कई जगह भीतर ही भीतर खीझता भी है—यही टोन इस फ्रैंचाइज़ की पहचान है।
कहानी जहां ताकत दिखाती है, वहीं कुछ ठोकरें खाती भी है। एक तीव्र, खिंचा हुआ गाना बीच में रफ्तार तोड़ देता है—ड्रामा का भाव तो आता है, पर फ्लो अटकता है। इसी तरह कैमल रेसिंग ट्रैक वाली दृश्य-संरचना थोड़ी बेमेल लगती है, जैसे कोई और फिल्म अचानक बीच में घुस आई हो। एक महत्वाकांक्षी कारोबारी का किरदार भी कुछ सपाट लिखा गया है—गुस्से और बदले के दायरे से बाहर निकलता नहीं, वरना फिल्म की नैतिक बहस और भी कई शेड्स पा सकती थी।
कोर्टरूम के अंदर के सीक्वेंस मज़ा देते हैं। सवाल-जवाब की रफ्तार तेज़ है, चुटकुले थोपे नहीं गए, और चालाक व्यंग्य अक्सर सबसे उंचे पंच देता है। सबूतों का खेल, गवाहों के बयान और जज की दखल—ये तीनों मिलकर एक ऐसी नाटकीय लय बनाते हैं जो दर्शक को सीट से चिपकाए रखती है।
दूसरे हाफ में अरशद वारसी का स्क्रीन-टाइम कुछ कम महसूस होता है। अच्छी बात यह कि फिल्म इस कमी को एक भावुक और स्मार्ट ट्विस्ट से संतुलित करती है—एक ऐसा पल जो बताता है कि यह टक्कर ‘किसका जोली बड़ा’ की होड़ से आगे है; मामला न्याय, नीयत और नींव का है।
क्लाइमैक्स में फिल्म शोर नहीं, सवाल चुनती है। बड़े-बड़े भाषण नहीं हैं; संवाद छोटे हैं, पर असरदार। सबसे तीखा प्रश्न यही उठता है—चॉइस आखिर किसकी जेब में रहती है? जिनके पास ताकत, पहुंच और पैसा है, उनके लिए विकल्प होते हैं; बाकी लोगों के हिस्से अक्सर मजबूरियाँ आती हैं। यह लाइन बस बयान नहीं, पूरी कहानी का नैतिक फ्रेम बन जाती है।
परफॉर्मेंस की बात करें, तो अक्षय कुमार स्टार-गुरुत्व से बाहर निकलकर किरदार की चाल-ढाल में घुसते हैं—दिखावा कम, टोन-कंट्रोल ज्यादा। अरशद वारसी अपनी खास ‘कॉमिक-विड’ के साथ आते हैं—मुस्कान में चोट छिपी, और चोट में मज़ाक। दोनों की जुगलबंदी दर्शक के लिए बोनस है; और जब भी सौरभ शुक्ला स्क्रीन पर आते हैं, यह तिकड़ी फिल्म को एक स्तर ऊपर ले जाती है।
लेखन की सबसे बड़ी जीत यह है कि फिल्म एक साथ तीन ट्रैक संभाल लेती है—मामले की कानूनी बारीकियाँ, आम आदमी का असली डर, और पॉपुलर एंटरटेनमेंट। कहीं-कहीं यह संतुलन हिलता है—गाना, बेमेल ट्रैक, और एक-आध सपाट किरदार इसकी मिसाल हैं—लेकिन कुल मिलाकर टोन अपनी जगह बना लेता है।
बैकग्राउंड स्कोर अदालत की चहल-पहल, तकरार और टर्निंग पॉइंट्स के साथ अच्छे से चलता है; हां, वही एक ‘इंटेंस’ गाना फ्लो तोड़ता है, जो कम किया जा सकता था। एडिटिंग फर्स्ट हाफ में चुस्त है; सेकंड हाफ के 20-25 मिनट ट्रिम होते तो अनुभव और कसैलापन पकड़ लेता।
फ्रैंचाइज़ संदर्भ में देखें, तो पहली फिल्म ने 2013 में कोर्टरूम व्यंग्य का एक टेम्पलेट बनाया था—छोटे शहर की खुशबू, मिडिल-क्लास का हीरो, और सिस्टम को आईना। दूसरी फिल्म में स्केल बड़ा हुआ, स्टार पावर आई, और टोन अधिक व्यावसायिक हो गया। तीसरा भाग इन दोनों दुनियाओं को जोड़ता है—सितारा भी है, सच्चाई भी; हंसी भी है, कड़वाहट भी। और सबसे अहम—सुभाष कपूर की वह ‘सीधे-सपाट’ आवाज़, जो मुद्दे को सिनेमाई बनाती है, पर मुद्दे की धार कुंद नहीं करती।
शोहरत की दुनिया में किसी फ्रैंचाइज़ का ‘क्यों’ अक्सर गायब हो जाता है। यहां ‘क्यों’ साफ है—सिस्टम से असहमति का अधिकार, न्याय की उम्मीद और आम-आदमी की थकी, मगर जिद्दी आवाज़। यही वजह है कि फिल्म दर्शकों को हर 16-18 मिनट पर ताली बजाने का मौका देती है; वे हंसते हैं क्योंकि चुटकुला अच्छा है, और ताली इसलिए बजाते हैं क्योंकि बात अंदर तक जाती है।
बॉक्स ऑफिस के शुरुआती संकेत मजबूत हैं। ट्रेड टॉकरों के मुताबिक पहले दिन 6 करोड़ के आसपास या उससे ऊपर की ओपनिंग की उम्मीदें जताई गईं, और शुरुआती शो पर दर्शकों की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही। इस तरह की ‘कोर्टरूम ड्रामेडी’ आमतौर पर वर्ड-ऑफ-माउथ पर उड़ती है—यह फिल्म उसी राह पर दिखती है।
क्या यह सबसे ‘रिफाइंड’ कोर्टरूम ड्रामा है? नहीं। क्या यह मनोरंजन और सामाजिक चेतना का इफेक्टिव कॉम्बो बनाती है? हां। यही संतुलन इस सीरीज़ को मायने देता है—यह मज़े भी कराती है और दिमाग भी काम पर लगाती है। परिवार के साथ बड़े पर्दे पर देखने लायक इसलिए है क्योंकि यह मज़ाक के बीच से सच निकालती है, और सच के बीच से उम्मीद।

किसके लिए, क्यों और कितनी मजबूती से
अगर आप कोर्टरूम की नोकझोंक, हल्की-फुल्की टांग-खींचाई, और मुद्दों की जैकेट में पैक्ड मनोरंजन पसंद करते हैं, यह फिल्म आपको जोड़े रखेगी। अक्षय- अरशद की टक्कर और सौरभ शुक्ला की मौजूदगी इसे परफॉर्मेंस-ड्रिवन शो बनाती है। हां, कुछ जगहें खटकती हैं—एक खिंचा गाना, एक बेमेल सबप्लॉट, और एक-आध कैरेक्टर की सपाटी—मगर फिल्म अपनी ऊर्जा, संवाद और ह्यूमर से बार-बार टोन सेट करती है।
सबसे दिलचस्प बात यह है कि क्लाइमैक्स बिना भारी-भरकम मोनोलॉग के असर छोड़ता है। ‘चॉइस’ बनाम ‘मजबूरी’ वाली बहस आपको थिएटर से बाहर आते वक्त भी पीछा करती है। यही वह आफ्टरटेस्ट है जो इस फ्रैंचाइज़ को बाकी से अलग खड़ा करता है—मनोरंजन के बीच नागरिकता का अहसास, और अदालत की चारदीवारी के भीतर जनता की आवाज़।



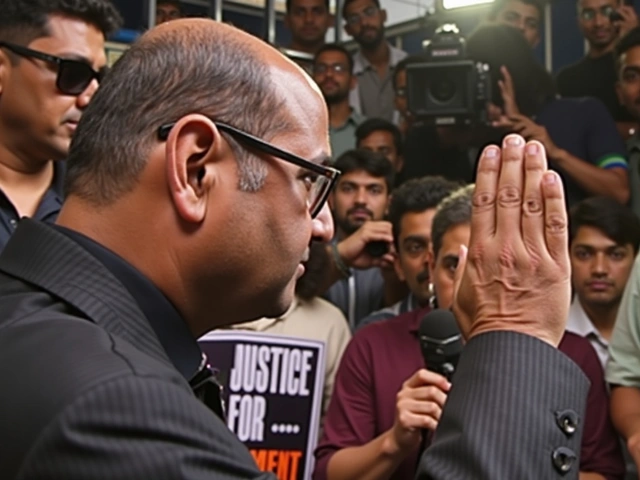

Hemant Kumar
bhool gaye kya ye film kisne banayi thi? jolly llb 1 mein jo mazak tha, wohi hai ab bhi... bas ab logon ne isse 'social commentary' ka naam de diya hai. 😅
NEEL Saraf
I loved how the film didn’t preach… it just showed. The farmer’s scene? I cried. Not because it was dramatic… but because it was true. And Akshay? He didn’t act. He just… was. ❤️
Ashwin Agrawal
The courtroom scenes were crisp. The pacing, the timing, the way the judge spoke - all felt real. Not like those Bollywood court dramas where lawyers shout for 10 minutes straight. This one? Real talk.
Shubham Yerpude
Let me be clear: this is not cinema. This is manufactured dissent. The film weaponizes agrarian distress for box office gain. The real issue? The system is not broken - it is being exploited by media-savvy elites to manufacture moral superiority. The ‘common man’ here is a prop. The real power lies in the production house.
Hardeep Kaur
I’m not a lawyer, but I’ve seen how courts work in small towns. The film got the small-town energy right - the pauses, the hesitations, the way people look away when they lie. That’s what made it feel real. Not the dialogues. The silence.
Chirag Desai
Arshad’s laugh? That’s the real hero. He makes you laugh, then you realize you’re laughing at yourself.
Abhi Patil
One must acknowledge the semiotic density of this cinematic artifact - the juxtaposition of the Uttar Pradesh dialects as a metaphor for the hegemonic linguistic stratification within the postcolonial judiciary. The ‘jolly’ persona is not comedic - it is a performative subversion of the bourgeois legal subject. The film’s climax, where choice is framed as a commodity, echoes Foucault’s biopolitical apparatus. One wonders if the director even knows this - or if it’s just lucky intuition.
Devi Rahmawati
I appreciate how the film avoided the trap of villainizing the system. Instead, it showed how individuals - judges, lawyers, even clients - are trapped within it. That’s the real tragedy. Not corruption. Complicity.
Prerna Darda
The film’s brilliance lies in its refusal to resolve. It doesn’t offer justice - it offers awareness. And in a country where systemic apathy is the norm, awareness is the first act of resistance. The song? A narrative disruption. But the silence after the climax? That’s the real soundtrack.
rohit majji
guys this movie is fire 🔥 seriously. akshay ki acting, arshad ki comedy, aur saurabh shukla ka judge? pure film ka heart. kuch jagah thoda slow tha lekin overall 10/10. jao dekho, bhaiyo aur behno!
Uday Teki
I cried at the end. Not because it was sad. But because I’ve seen that moment in real life. And no one ever wins. 😢